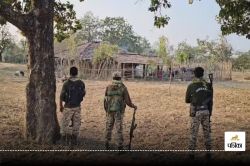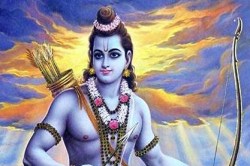Sunday, April 6, 2025
पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – पौरुष-शील के पर्याय राम-सीता
राम इक्ष्वाकु वंश के थे। गीता ज्ञान त्रेतायुग में भी उपलब्ध था। क्यों नहीं—राम और कृष्ण बाहर दो थे, भीतर तो एक ही थे। दोनों विष्णु के ही अवतार थे।
जयपुर•Apr 06, 2025 / 07:32 am•
Gulab Kothari
गुलाब कोठारी इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्।। (गीता 4.1) -मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने मनु से और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। राम इक्ष्वाकु वंश के थे। गीता ज्ञान त्रेतायुग में भी उपलब्ध था। क्यों नहीं—राम और कृष्ण बाहर दो थे, भीतर तो एक ही थे। दोनों विष्णु के ही अवतार थे। राम आग्नेय स्वरूप-सूर्यवंशी थे, तो कृष्ण सौम्यता के प्रतिमान-चन्द्रवंशी थे। अग्नि-सोम ही तो सृष्टि के मूल तत्त्व हैं। दोनों के अवतार का भी एक ही कारण रहा—यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत….।
संबंधित खबरें
राम को सूर्य/इन्द्र के स्वरूप में देखने की आवश्यकता है। सूर्य जगत का आत्मा है, पिता है, अग्नि-वायु-आदित्य (वैश्वानर) भी अग्नि के ही घन-तरल-विरल रूप हैं। घनात्मक रूप ही सत्य (सगुण) सृष्टि का विकास है। सूर्य न केवल विष्णु का अवतार है, बल्कि साक्षात विष्णु की (श्रद्धा सोम रूप) सविताग्नि में आहुति से उत्पन्न हुआ (पुत्र) है।
निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च (ऋ.1.35.2)—सबको अपने-अपने कर्म में लगाने वाला गृहस्थ धर्म का आदर्श उदाहरण भी है। अनासक्त पुरुषार्थ योग रामावतार का आदर्श कहा जाता है। आधिदेविक धरातल पर देवासुर संग्राम को भी प्रतिबिम्बित करता है। सूर्य ही सत्य नारायण विष्णु है। अग्नि-सोमात्मक जगत के प्रथम प्रतीक है। इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी था। सूर्य ऋत का नियामक है सविता रूप में और पारमेष्ठ्य ऋत का अनुगामी है। रावण ऋत को स्वीकार नहीं करता था, अत: अनृत का प्रतीक था। सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या। (शत.ब्रा. 3.9.4.1)
सविता वै देवानां प्रसविता। (शत.ब्रा. 1.1.2.17) सविता की इस प्रसविनी शक्ति (श्री) का वरुण की सृष्टि विरोधी तमस शक्ति द्वारा अपहरण करने की कुचेष्टा और परिणाम स्वरूप देवासुर-संग्राम।
यह भी पढ़ें
राम की वीरता में नौ गुणों की स्थापना है- विजिगीषा, रक्षा, दीप्ति, प्रचोदन (प्रेरणा), करुणा, पुरुषार्थ, शबलता, भूमा, और ऐश्वर्य। जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, वैसी ही भूमिका प्रकट हुई। कैकयी संवाद, भरत संवाद, केवट संवाद, बाली या फिर शबरी संवाद, समुद्र पर क्रोधित-आग्नेय स्वरूप, सीता-विरह विलाप भी और सीता के लौट आने पर ठुकरा देना भी। न राग, न द्वेष, धरती फटी, सीता समा गई, और राम?
राम शब्द में ‘रा’ अग्नि सूचक है जो कि रावण में भी था। किन्तु ‘म’ की भूमिका रावण के ‘वन’ को जलाने के ही काम आई। यूं तो रामायण को पारिवारिक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, भोग-त्याग के मूल्यों की प्रति भी है, पत्नी के महत्त्व को बढ़ाया भी है और शंकित रूप में निम्न कोटि में भी डाला है।
यह भी पढ़ें
राम मर्यादा पुरुष थे। एक ओर श्री (लक्ष्मी) दूसरी ओर सरस्वती (शब्द मर्यादा)। ‘रघकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई’—आज तक श्रेष्ठतम उदाहरण बना बैठा है। राम की सौम्यता के उदाहरण कृष्ण से कम हैं, आग्नेय-दृढ़ता-तटस्थता के उदाहरण अधिक हैं। राम स्वंय के लिए नहीं जिए। गीता का सन्देश उनके जीवन में भी प्रभावी रहा—धर्म सस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे।
इस एक उद्देश्य को ही शाश्वत स्वरूप दिया। इसके आगे शेष सबकुछ नश्वर था। राजपाट-व्यक्ति-समाज। राजनीति-कूटनीति में राम प्रवीण थे। पौरुष के प्रतिबिम्ब थे। कृष्ण में परोक्षवाद की झलक अधिक थी। कृष्ण की तरह राम ने अपनी दिव्यता का परिचय स्थान-स्थान पर नहीं दिया, किन्तु जब भी दिया, मानो भूचाल आ गया हो।
महापुरुष जितने भी होते हैं, जितने भी अवतार जन्म लेते हैं, वे देव-असुर सम्पदा सहित ‘प्रोग्राम’ लेकर आते हैं। उनके कार्यों में परिवर्तन संभव नहीं है। न राम कुछ अलग कर सकते हैं, न ही सीता कुछ बदल सकती है। न कैकेयी, न रावण, न बाली, न ही सुग्रीव। हनुमान तो चिरंजीवी हो गए। राम को साधारण मानव की भांति देखना पहली जरूरत है। सीता को भारतीय धर्मपत्नी के रूप में (शास्त्र सम्मत) देखना होगा। चौदह वर्ष वन में राम के साथ रहना भी सीता का ही निर्णय था और अग्नि परीक्षा का निर्णय भी सीता का ही था। राम के किसी भी निर्णय के लिए सीता ने कभी उलाहना नहीं दिया। न ही लव-कुश को राम के विरुद्ध कोई ताड़ना का भाव जताया।
राम यदि साधारण मानव की तरह सीता के साथ व्यवहार कर रहे थे, तभी तो सीता के साहस-सतीत्व-मानव रूप मर्यादा को प्रकट होने का (अभिव्यक्ति का) अवसर मिला। ‘‘यदि आप मुझे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हैं, तो मेरा जीने का अर्थ ही क्या रह जायेगा।’’ और सीता ने लक्ष्मण को चिता तैयार करने का आदेश दे दिया। न राम से अनुनय-विनय की, न ही अन्य से सहायता मांगी।
यह भी पढ़ें
सीता ने साहसपूर्वक वंश मर्यादा का उदाहरण पेश किया। लव-कुश ने भी मां-बाप की भूमिका को परिस्थिति-जन्य ही माना। पुत्रों में राम के बीज को ही पल्लवित किया। तभी तो वे खेल-खेल में राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक सके। इस बात को साधारण धोबी कैसे समझता कि राक्षसों के बीच वर्षों रहकर भी सीता सुरक्षित थी। राम पौरुष और सीता शील का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम भी यदि राम को साधारण मानव रूप में देखें तो अर्थ बदल जाएंगे। हम राम को अवतार से कम देखना ही नहीं चाहते। सीता के एक आह्वान पर पृथ्वी देवी उन्हें लेने आ गई, और सीता पाताल में समा गई! राम धन्य हुए या सीता?
gulabkothari@epatrika.com
Hindi News / Opinion / पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – पौरुष-शील के पर्याय राम-सीता
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
ओपिनियन
बाजार क्यों हो स्वास्थ्य नीतियों का निर्धारक
4 minutes ago
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.