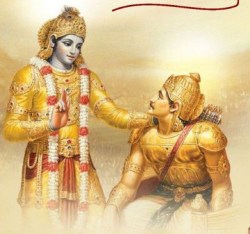Saturday, April 19, 2025
मुद्दा: मर्यादित आचरण से ही बचेगी संवैधानिक पदों की गरिमा
— राज कुमार सिंह
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
जयपुर•Apr 17, 2025 / 11:32 am•
विकास माथुर
पहली बार किसी राज्य में राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी बिना ही कानून लागू हो गए। तमिलनाडु में एमके स्टालिन सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को, राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी बिना ही, अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह स्थिति तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा इन विधेयकों को मंजूरी के लिए लंबे समय से लटकाए रखने और फिर राष्ट्रपति को भेज देने के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से उत्पन्न हुई है।
संबंधित खबरें
न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और न्यायाधीश आर. महादेवन की पीठ ने इन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वीकृत घोषित कर विधेयकों पर निर्णय के लिए एक से तीन माह की समय सीमा भी तय कर दी। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी विधेयक को राज्यपाल अनिश्चितकाल तक अपने पास रोके नहीं रख सकते। यह भी कि विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर भेजे गए विधेयकों को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प राज्यपाल के पास नहीं है। ऐसे विधेयकों को राज्यपाल, राष्ट्रपति को भी नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति को भी अपने पास भेजे गए विधेयकों पर तीन माह में फैसला करना होगा।
बेशक विधेयकों की संवैधानिक वैधता पर राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि राज्यपालों के पास ऐसा कोई तंत्र उपलब्ध नहीं, पर उससे अधिक समय लगने पर राज्य सरकार को कारण बताने पड़ेंगे। न्यायालय ने राज्यों से भी कहा है कि वे केंद्र के प्रश्नों और सुझावों पर सहयोगात्मक रुख अपनाएं। निर्वाचित राज्य सरकारों और राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि राज्यपाल के बीच टकराव नया नहीं, पर उच्चतम न्यायालय से ऐसा मार्गदर्शक निर्णय पहली बार आया है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। उनसे अपेक्षा रहती है कि वह अपने सत्तारूढ़ दल की पृष्ठभूमि या उससे निकटता के बावजूद संविधान के दायरे में भूमिका का निर्वाह करें।
तमिलनाडु मामले में उच्चतम न्यायालय को नसीहत देनी पड़ी कि राज्यपाल को राज्य के मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ से निर्देशित होना चाहिए। यह भी कि राज्यपाल समस्याओं के समाधान का अग्रदूत होता है, उसे उत्प्रेरक होना चाहिए, न कि अवरोधक। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रखना ‘अवैध’ है और इसे ‘रद्द’ किया जाना चाहिए। यह भी कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास ‘वीटो पावर’ नहीं है। तमिलनाडु विधानमंडल ने जनवरी, 2020 से अप्रेेल, 2023 के बीच संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के लिए 12 विधेयक भेजे, जिनमें से ज्यादातर राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों से संबंधित थे, लेकिन रवि उन्हें लटकाकर बैठ गए। नवंबर, 2023 में जब तमिलनाडु सरकार उच्चतम न्यायालय चली गई तो उन्होंने दो विधेयक राष्ट्रपति को भेजकर 10 विधेयक रोक लिए। विधानसभा ने वे 10 विधेयक दोबारा पारित कर मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजे, तो उन्होंने वे सभी राष्ट्रपति के पास भेज दिए। राष्ट्रपति ने एक विधेयक को मंजूरी दी, तो सात को खारिज कर दिया, जबकि शेष दो प्रस्तावित कानूनों पर विचार ही नहीं किया। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह देश में इकलौता मामला नहीं है। जिन राज्यों में भी केंद्र से अलग राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार है, वहीं ऐसे विवाद नजर आना ही बहुत कुछ कह देता है। राज्यपाल और निर्वाचित राज्य सरकार में अशोभनीय टकराव लोकतंत्र और संघवाद के लिए सुखद नहीं। दरअसल, राज्यपाल चुनाव में पराजित या बुजुर्ग राजनेता अथवा केंद्र सरकार के चहेते पूर्व नौकरशाह आदि होते हैं। इसलिए भी वे दूसरे राजनीतिक दल की राज्य सरकार को परेशान कर अपने आकाओं को खुश करने में कसर नहीं छोड़ते।
राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों की सुविधाजनक व्याख्या कर निर्वाचित राज्य सरकारों के कामकाज में अडंगे लगाते हैं। अतीत में वे सरकारों को बर्खास्त कर अपने आकाओं की मनपसंद सरकार बनाने की हद तक जाते रहे हैं। राज्यपाल को मोहरा बनाकर विपक्ष की राज्य सरकारों को अस्थिर करने का खेल आजादी के बाद ही शुरू हो गया था, जब 1958 में केरल में शिक्षा में बदलाव संबंधी आंदोलन की आड़ लेकर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए राज्यपाल ने विधानसभा में बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद की वामपंथी सरकार बर्खास्त कर दी। 1967 में राज्यपाल धर्मवीर ने पश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी की बहुमत प्राप्त वामपंथी सरकार को बर्खास्त कर वहां पीसी घोष के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित सरकार बनवा दी। 1977 और 1980 में तो यह जैसे ‘म्यूजिकल चेयर गेम’ बन गया।
आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ हुई तो कई कांग्रेस शासित राज्य सरकारें बर्खास्त कर राज्यपाल भी हटा दिए गए। 1980 में सत्ता में वापसी पर इंदिरा गांधी ने भी उसी अंदाज में हिसाब चुकता किया। संवैधानिक पदों की गिरती गरिमा को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही बचाया जा सकता है।
Hindi News / Opinion / मुद्दा: मर्यादित आचरण से ही बचेगी संवैधानिक पदों की गरिमा
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.